प्रचंड धधकती हुई घूप और 43 डिग्री से ऊपर तापमान, यही है भारत के अधिकाँश भाग में ग्रीष्म ऋतु यानि गर्मी के मौसम का हाल। गर्मी के मौसम की विशेषता है उच्च तापमान। दिन लम्बे हो रहे हैं और तापमान बढ़ रहा है। भारत में गर्मी का मौसम आम तौर पर मार्च से जून तक होता है। यहाँ अधिकतम तापमान 40°C से 50°C तक और न्यूनतम तापमान 20°C से 30°C तक हो सकता है लेकिन क्षेत्र के आधार पर भिन्नता हो सकती है। समुद्र के प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्र में गर्मी के साथ-साथ उमस भी होती है जिससे और अधिक असहजता का अनुभव होता है।
क्षेत्रीय भिन्नता:
- उत्तर भारत: यहाँ गर्मियों में तापमान बहुत अधिक होता है, विशेषकर पश्चिमी और मध्य भागों में।
- दक्षिण भारत: यहाँ का तापमान औसत रूप से कम होता है, विशेषकर पश्चिमी घाट क्षेत्र में।
- पूर्वी भारत: यहाँ का तापमान उत्तर भारत की तुलना में कम होता है, लेकिन दक्षिण भारत की तुलना में अधिक होता है।
- पहाड़ी क्षेत्र: यहां का तापमान मैदानी क्षेत्र की तुलना में काफी कम होता है।
कुछ क्षेत्र में, धूल भरी आँधी या " लू " भी आती है। ये हलके तूफ़ान की तरह गर्म, धूलभरी हवाएं होती हैं जिनसे दृश्यता कम हो सकती है और श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
गर्मी में होने वाली सामान्य बीमारियाँ:
चिलचिलाती धूप और गर्मी से कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं। भारत में गर्मियों की आम बीमारियाँ, क्षेत्र, जलवायु और व्यक्तिगत स्वास्थ्य जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। आइए, इन आम चुनौतियों तथा इनके उपायों के बारे में जानें:
- डाइहाइड्रेशन (निर्जलीकरण): गर्मी में पसीने की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे मुँह में सूखापन, प्यास, थकान, चक्कर आना, सिरदर्द, पेशाब कम आना या गहरे रंग का होना और भ्रम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। नैट्रम म्यूर, नैट्रम कार्ब, चाइना, एसिड फॉस आदि सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली होमियोपैथिक औषधियाँ हैं।
- हीट स्ट्रोक (लू लगना): गर्मी के महीनों के दौरान तापमान बढ़ने के साथ, हीटस्ट्रोक (जिसे लू लगना कहते हैं) एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन जाता है। यह तब होता है जब लंबे समय तक उच्च तापमान के संपर्क में रहने के कारण शरीर गर्म हो जाता है और इससे शरीर का उच्च तापमान, तेज़ दिल की धड़कन, तेज़ सिरदर्द, चक्कर आना, मतली, कमजोरी, उल्टी, भ्रम और बेचैनी जैसे लक्षण शामिल होते हैं। ऐसे में अमाइल नाइट्रिकम, बैलाडोना, एकोनाइट, जैल्सीमियम, ग्लोनाइन, लैकेसिस, नैट्रम कार्ब, सोल, वैरेट्रम एल्ब आदि का प्रयोग किया जाता है।
- सनबर्न: धूप में बिना सुरक्षा के रहने से त्वचा झुलस-कर लाल रंग की हो जाती है, जिसे सनबर्न कहते हैं। यह सूर्य की पराबैंगनी (यू.वी.) किरणों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से हो सकता है, जिसकी विशेषता लाल, दर्दनाक त्वचा होती है जिसपर छाले पड़ सकते हैं अथवा वह जल्दी छिल सकती है। इससे त्वचा कैंसर और समय से पहले बूढ़ा होने का खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पर इससे त्वचा में दर्द और जलन होती है। अगैरिकस, ऐंटिम क्रूड, कैंमफर, कैन्थरिस, मुरिएटिक एसिड, नैट्रम कार्ब, पल्सैटिल्ला, सोल, थूजा, अर्टिका युरेन्स आदि सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली होमियोपैथिक औषधियाँ हैं।
- घमौरियां (Prickly heat or Miliary rash): इसे घमौरियां या मिलिया के रूप में भी जाना जाता है, घमौरियां तब होती हैं जब पसीने की नलिकाऐं अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे त्वचा पर छोटे-छोटे लाल दाने या छाले हो जाते हैं। यह गर्मियों में होना आम बात है। इससे खुजली होती है और जलन महसूस होती है। ऐसे में एपिस, कैलेंडुला, बैलाडोना, कैन्थरिस, नैट्रम कार्ब, पल्सैटिल्ला, सोल, थूजा, अर्टिका युरेन्स, वैलेरियाना आदि का प्रयोग किया जाता है।
- आंखों में संक्रमण (Eye infection): धूल-मिट्टी और गर्मी के कारण आंखों में संक्रमण हो सकता है। गर्मियों में आंखों में संक्रमण अधिक आम हो सकता है क्योंकि लोग बाहर अधिक समय बिताते हैं और स्विमिंग पूल में क्लोरीन जैसे जलन पैदा करने वाले पदार्थों के संपर्क में आने की संभावना अधिक होती है। इससे आंखों में जलन, खुजली, लालिमा और आंखों से पानी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में बैलाडोना, यूफ्रेशिया, एपिस आदि सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली होमियोपैथिक औषधियाँ हैं।
- फूड पॉइजनिंग (Food poisoning): गर्म तापमान में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, जिससे दूषित या बासा भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके रोगी अक्सर उल्टी और बुखार के लिए अस्पताल जाते हैं। गर्मियों के दिनों में ऐसे रोगियों से अस्पताल भरे पड़े रहते हैं। इसके मुख्य लक्षणों में जी मिचलाना, उल्टी, पेट दर्द, पेट में ऐंठन, दस्त, बुखार और शरीर में दर्द आदि होते हैं। ऐसे में लक्षणों के आधार पर ऐंटिम क्रूड, आर्सेनिक एल्ब, ईपीकाक, मर्क सौल, वेराट्रम एल्ब आदि का उपयोग किया जाता है।
- गले में ख़राश (Sore throat or Pharyngitis): गर्म तापमान में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, इन्हीं में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस (GAS) एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो त्वचा और श्वसन पथ से संक्रमण का कारण बन सकता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सांस की बूंदों जैसे कि खांसने या छींकने से और बैक्टीरिया से दूषित त्वचा या अन्य सतहों को छूने से फैलता है। इसके संक्रमण से गले में ख़राश, गुटकने में परेशानी, आवाज़ बैठना (लैरिनजाइटिस), बुखार, खांसी या कभी-कभी टॉन्सिल्स आदि भी हो सकते हैं। ऐसे में लक्षणों के आधार पर बैलाडोना, लाइकोपोडियम, एपिस, बैरायटा-कार्ब, बैरायटा-म्यूर आदि का उपयोग किया जाता है।
- जल-जनित और भोजन-जनित रोग: (Water-borne and food-borne diseases) गर्मियों में अस्वच्छ पेयजल और दूषित भोजन से जल-जनित और भोजन-जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ये वे बीमारियाँ हैं जो दूषित पानी पीने अथवा दूषित भोजन खाने से होती हैं। इन बीमारियों या स्थितियों में दस्त (Diarrhoea), पेचिश (Dysentery), हैजा (Cholera), टाइफाइड (Typhoid), जिआर्डाएसिस (Giardiasis), हेपेटाइटिस-ए (Hepatitis A), पीलिया (Jaundice) आदि शामिल हैं। जल-जनित और भोजन-जनित रोगों के मुख्य लक्षण: पेट दर्द, मरोड़, मितली, उल्टी, दस्त, बुखार, कमजोरी, आदि हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में और बचाव के उपायों के बारे में:
- जल-जनित रोग: दूषित पानी पीने, दूषित पानी में नहाने या उससे धोए हुए भोजन को खाने से फैलने वाले रोग जल-जनित रोग कहलाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी इन रोगों को फैलाने वाले मुख्य कारक हैं।
- भोजन-जनित रोग: दूषित या अधपका भोजन खाने से फैलने वाले रोग भोजन-जनित रोग कहलाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन (विष) इन रोगों को फैलाने वाले मुख्य कारक हैं, जिनके कुछ उदाहरण हैं साल्मोनेला (Salmonella), ई.कोलाई (E. coli), नोरोवायरस (Norovirus), स्टेफाईलोकोकस ऑरियस (Staphylococcus aureus),आदि।
डायरिया (दस्त): गर्मी में अस्वच्छ पेयजल या दूषित भोजन से डायरिया की समस्या हो सकती है। इसके लक्षणों में बार-बार पानी जैसा मल होना, पेट में मरोड़ और शरीर में डिहाइड्रेशन शामिल हैं।
टाइफाइड: यह दूषित पानी और भोजन से फैलता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, थकान, कमजोरी, पेट दर्द, सिरदर्द और भूख न लगना आदि शामिल हैं।
बचाव के उपाय:
- हमेशा साफ और शुद्ध पानी पिएं।
- उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिएं।
- फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही खाएं।
- बाजार से कटे हुए फल या सब्जियां लेने से बचें।
- गर्म खाना ही खाएं।
- मांस, मछली और अंडों को अच्छी तरह पकाएं।
- रसोई और बर्तनों को साफ रखें।
- परजीवी जनित बीमारी (Vector-borne diseases): वेक्टर-जनित रोग वे रोग होते हैं जो वेक्टर या कीट, कीटाणु या अन्य प्राणियों द्वारा प्रसारित होते हैं। इन रोगों का प्रसार मुख्य रूप से मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, आदि के माध्यम से होता है। ये रोग आमतौर पर गर्मी के मौसम में अधिक होते हैं। कुछ मुख्य वेक्टर-जनित रोग हैं:डेंगू बुखार: डेंगू एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है जो भारत में आम है। लक्षणों में तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकान, मितली, उल्टी और त्वचा पर लाल चकत्ते शामिल हैं। गंभीर होने पर इसमें प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं जिससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। होमियोपैथी में डेंगू के लिए यूपीटोरियम पर्फ सबसे प्रसिद्ध दवा है। डेंगू में सर्पविष से बनी औषधियों का भी उपयोग बाद के चरणों में किया जाता है जब गंभीर रक्तस्राव शुरू हो जाता है।मलेरिया: मलेरिया मादा एनोफेलीज़ मच्छर के काटने से होने वाली एक गंभीर बीमारी है जिसमें बुखार, थकान और लीवर तथा स्प्लीन सम्बन्धी समस्या होती है।
गर्मी से बचाव के उपाय:
गर्मी का मौसम आते ही तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना जरूरी होता है। आइये जानते हैं गर्मी से बचने के कुछ आसान उपायों के बारे में:
- शरीर को हाइड्रेट रखें: प्यास लगने से पहले ही पानी पीते रहें। दिन भर में कम से कम 2-3 लीटर पानी पिएं। पानी के अलावा नारियल पानी, छाछ, लस्सी जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें। फलों में तरबूज, खरबूजा, खीरा आदि पानी की मात्रा अधिक होती है, इन्हें अपने आहार में शामिल करें।
- कपड़ों का चुनाव: ढीले-ढाले और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। ये पसीने को सोखने में मदद करते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं। गहरे रंगों के कपड़ों से बचें, ये गर्मी को ज्यादा सोखते हैं।
- धूप से बचाव: दोपहर के समय जब धूप सबसे तेज होती है, तब घर से बाहर निकलने से बचें। यदि बाहर निकलना जरूरी हो तो छाता, टोपी और धूप का चश्मा लगाएं। सनस्क्रीन लोशन लगाकर त्वचा को सूरज की किरणों से बचाएं।
- खाने-पीने का ध्यान रखें: गर्मियों में भारी और ज्यादा मसालेदार भोजन से परहेज करें। हल्का और सुपाच्य भोजन खाएं। गर्मी से बचने के लिए दही, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, बेल का शरबत आदि ठंडे पेय पदार्थ का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें तथा रसीले फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा आदि का सेवन करें।
- मच्छरों से बचाव करें: रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, आदि को पनपने से रोके। अपने आसपास पानी जमा न होने दें ताकि मच्छर पनपें ही नहीं। बाजार में मच्छर भगाने के लिए कई तरह के उत्पाद मिलते हैं लेकिन आप उन्हें कुछ घरेलु उपायों को अपनाकर भी भगा सकते हैं। शाम होते ही नीम के तेल की कुछ बूँदें डालकर कपूर लौंग आदि का धुआं करें। सिट्रोनेला कैंडल आदि जलाएं और फिर भी यदि आपको लगता है कि आप ही को मच्छर ज़्यादा काटते हैं तो कुछ होमियोपैथिक दवाएं आती हैं जिन्हें लेने के बाद इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसके बारे में अपने नज़दीकी होमियोपैथिक चिकित्सक से बात करें।
- एयर कंडिशनर (AC) का उपयोग कम करें: हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और शरीर 23 डिग्री से लेकर 39 डिग्री तक का तापमान आसानी से सहन कर सकता है। जब आप AC को 19-20-21 डिग्री पर चलाते हैं तो कमरे का तापमान सामान्य शरीर के तापमान से बहुत कम होता है तो छींकने, कंपकंपी आदि से शरीर प्रतिक्रिया करता है तथा जिससे शरीर में हाइपोथर्मिया नामक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो रक्त परिसंचरण को प्रभावित करती है। शरीर के कुछ हिस्सों में रक्त की आपूर्ति प्रर्याप्त नहीं होती है जिससे लंबी अवधि में कई नुकसान और रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। AC चलाने पर अकसर पसीना नहीं आता है, इसलिए शरीर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं और लंबे समय में कई बीमारियों का खतरा होता है जैसे त्वचा की एलर्जी या खुजली, साल भर सर्दी-जुखाम बने रहना, साइनोसाइटिस, अडेनोइड्स, विटामिन डी की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना और यहाँ तक कि उच्च रक्तचाप, गठिया, आदि भी। इसके साथ ही इससे अत्यधिक बिजली की खपत भी होती है। अतः AC आपकी सेहत खराब करने के साथ, आपकी जेब से पैसा भी उड़ाता है और पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग भी करता है। कोशिश करिए कि AC के बजाए कूलर या फिर खस पर्दों का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा समय हवादार कमरे में बिताएं, जिससे शरीर में विटामिन डी की कमी न होने पाए। यदि यह संभव न हो सके तो AC चलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे 24 से 26 डिग्री पर चलाएं और इसके साथ पंखे को धीमी गति से चलाएं। इससे बिजली तो कम खर्च होगी ही साथ ही आपके शरीर का तापमान भी सीमा में रहेगा और आपकी सेहत पर कोई बुरा असर भी नहीं पड़ेगा। इसका एक और फायदा यह है कि इससे अंततः ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करके पर्यावरण को बचने में भी मदद मिलेगी।
- अन्य उपाय: घर को ठंडा रखने के उपाय करें जैसे छोटे पौधे लगाना, पर्दे लगाना, खिड़कियों पर शेड लगाना आदि। नियमित रूप से स्नान करें। बहुत ठंडे पेय पदार्थ पीने से बचें।
होमियोपैथी हो सकती है मददगार:
गर्मी का मौसम आते ही बच्चों को स्कूल की छुट्टियों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लेकिन कई बार बीमारियों के कारण छुट्टियों का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। गर्मी के दिनों में भारत में कई तरह की बीमारियां अपने पैर पसारने लगतीं हैं। गर्मी के मौसम में उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, यह छुट्टियों, यात्रा और बाहरी गतिविधियों जैसे पिकनिक, तैराकी, लंबी पैदल यात्रा और बेसबॉल, सॉकर या क्रिकेट जैसे खेलों में शामिल होने का भी समय है। कुछ आसान उपायों तथा होमियोपैथी को अपनाकर आप गर्मी के मौसम में भी स्वस्थ और तरोताजा रह सकते हैं। होमियोपैथी उपरोक्त सभी प्रकार की समस्याओं से निपटने में अत्यधिक प्रभावी है। चिकित्सक मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और लक्षणों के आधार पर, समस्या के कारणों का निर्धारण करते हैं तथा इसी के आधार पर दवा का चुनाव किया जाता है। गर्मियों में होने वाली यह आम बीमारियों में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली दवाओं में एकोनाइट, अमाइल नाइट्रिकम, एलियम सीपा, आर्सेनिक एल्ब, ब्रायोनिया, बैलाडोना, बैपटीसीया, जैल्सीमियम, ग्लोनाइन, लैकेसिस, नैट्रम कार्ब, नाइट्रिक एसिड, पल्सैटिल्ला, सोल, वैलेरियाना, आदि शामिल हैं।
उचित स्वच्छता बनाए रखने और समय पर अपने निकटतम होमियोपैथ के पास जाने से आप अनावश्यक अस्पताल के दौरे और दीर्घकालिक बीमारी से बच सकते हैं। स्वयं अपना निदान और दवा का चयन एवं सेवन करने से बचें क्योंकि यह हानिकारक हो सकता है। कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा एक योग्य होमियोपैथिक चिकित्सक से परामर्श लें। होमियोपैथिक डॉक्टर प्रभावी उपचार के लिए अपने सभी रोगियों को आहार और जीवनशैली में कुछ बदलाव करने का सुझाव देते हैं। खास बात यह है कि होमियोपैथिक दवाओं को इत्र, कपूर, या अन्य वाष्पशील उत्पादों के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दवाओं के प्रभाव को बेअसर करती हैं। ऑनलाइन परामर्श या किसी भी संबंधित प्रश्न के लिए हमारे विशेषज्ञ होमियोपैथिक डॉक्टरों से परामर्श लें और हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करें।
नोट: इस लेख में दी गयी जानकारी के परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान या जोखिम, के लिए लेखक जिम्मेदार नहीं है। यह जानकारी किसी पेशेवर चिकित्सिए परामर्श, निदान अथवा उपचार का विकल्प नहीं है।


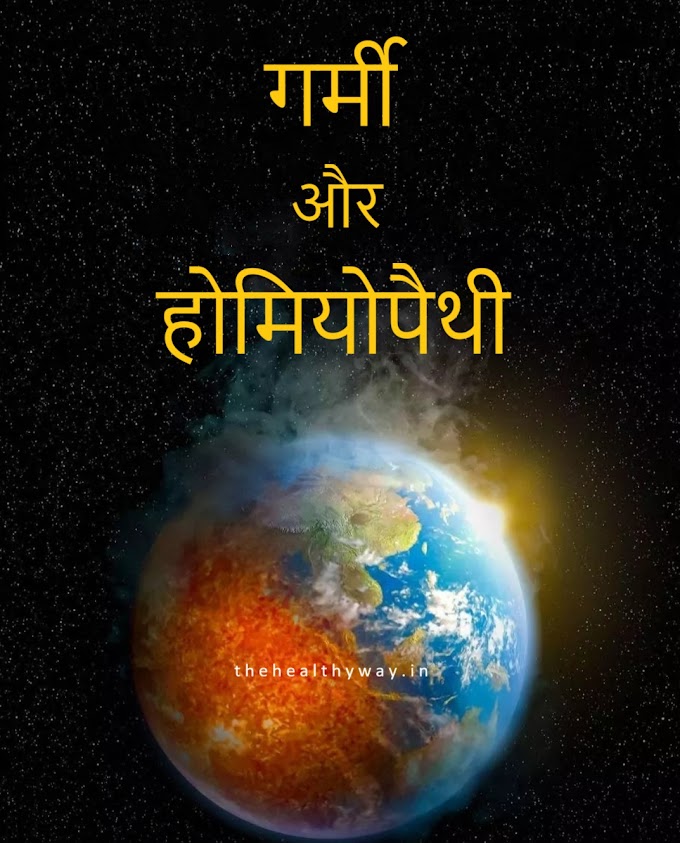


एक टिप्पणी भेजें